खबर वालों को खबर क्या ( आलेख ) डॉ लोक सेतिया
अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जो कभी ठोस वास्तविकता रही है । मीडिया टीवी चैनल अख़बार सभी राजनेताओं के भाषणों की बात सुनकर इतिहास इतिहास की रट लगाते रहते हैं मगर शायद ही कभी खबर के इतिहास की बात याद की हो किसी ने । इतिहास तो क्या अपना चेहरा तक भूल गये लगते हैं । आज किसी को याद नहीं होगा कि गांधी जी भी कभी अख़बार निकाला करते थे और देश की आज़ादी के आंदोलन में अख़बारों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है । बाबू बालमुकंद गुप्त जी का नाम भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा जो भारत में पत्रकारिता के पुरोधा माने जाते हैं और आज भी उनके नाम से इक पत्रिका नारनौल से बाबूजी का भारतमित्र नाम से निकलती है जिसके संपादक मेरे मित्र श्री रघुविंद्र यादव जी हैं । बाबू बालमुकंद गुप्त जी हरियाणा की भूमि की ही संतान थे , उनका जन्म हरियाणा के गुडियानी गांव में हुआ था ।
आज़ादी से पहले ही नहीं उसके बाद 1975 तक भी अख़बार कोई व्यापार नहीं इक अंदोलन हुआ करता था । तब अख़बार जागरूकता फ़ैलाने और सच को उजागर करने का काम किया करते थे और बहुत जोखिम उठाकर घोटालों की खोज करते थे । खबर की वास्तविक परिभाषा ही यही है :-
खबर वो सूचना है जो कोई जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा
और पत्रकार का काम है उसका पता लगा कर आम जनता तक सूचना पहुंचाना ।
ये सोचकर अजीब लगता है कि आजकल खबर उसे कहा जाने लगा है जो सरकार नेता अथवा बाकी लोग शोर मचा मचा कर बता रहे हैं । वो खबर कैसे है , खबर वालों को खुद अपनी खबर नहीं है । इक और शब्द पीत पत्रकारिता हुआ करता था जिसका अर्थ समझा जाता था कि जब कोई खबर किसी के कहने पर या अपने फायदे की खातिर बनाई जाए तो वो पीत पत्रकारिता होती है । उस नज़र से आज की पत्रकारिता पूरी की पूरी पीलिया रोग से पीड़ित है । खबर वास्तव में कोई देखने की वस्तु नहीं होनी चाहिए टीवी पर जो दिखाई जाती और जैसे दिखलाते हैं उस में खबर कहां खो गई या कत्ल कर दी गई कोई नहीं जान पाता है । टीवी सिनेमा की तरह इक मनोरंजन का माध्यम है और खबर को मनोरंजन बनाना किसी अपराध की तरह ही है । टीवी चैनल वालों को दोष नहीं देना चाहता , अख़बार वालों से गिला है । प्रसार संख्या और विज्ञापनों के मोहजाल ने उनको अपनी राह से ही भटका दिया है । सब से अधिक बुरा हुआ है टीवी और अख़बार दोनों के सरकारी विज्ञापनों के मोहजाल में फंस पर सच झूठ की पहचान भुला बैठे हैं ।
बैसाखियों के सहारे
सब बोलते हैं हम तेज़ दौड़ रहे हैं मगर बिना सरकारी बैसाखियों के दो कदम नहीं चलते सभी । काश ये सब नहीं हुआ होता और अख़बार अपने आप को कारोबार नहीं जनहित का अंदोलन मानते तो शायद केवल अपना ही नहीं राजनीति से लेकर धर्म और समाज तक की गिरावट को रोका जा सकता था । बहुत बहस करते हैं हर समाचार को लेकर , कभी खुद खबर की दुर्दशा पर भी चिंतन किया जाता । खबर जाने खो गई है या फिर थक कर सो गई है खबर वालों ने सच से नाता तोड़ लिया है घबरा कर लहरों से कश्ती का रुख किसी किनारे की तरफ मोड़ लिया है डूबना नहीं चाहते हौंसलों से तैरना छोड़ दिया है । खबर वाले कहते हैं सब की खबर रखते हैं , कौन जाने किस तरफ तिरछी नज़र रखते हैं , खुद अपनी खबर नहीं जिनको वो बिना दीवार दर का कोई घर रखते हैं । बैठे हैं थककर कहीं जारी मगर इक सफ़र रखते हैं जनता का भरोसा किसी पर भी नहीं , उनका नाता दोनों से है चोर सिपाही कब कौन खामोश अधर रखते हैं ।
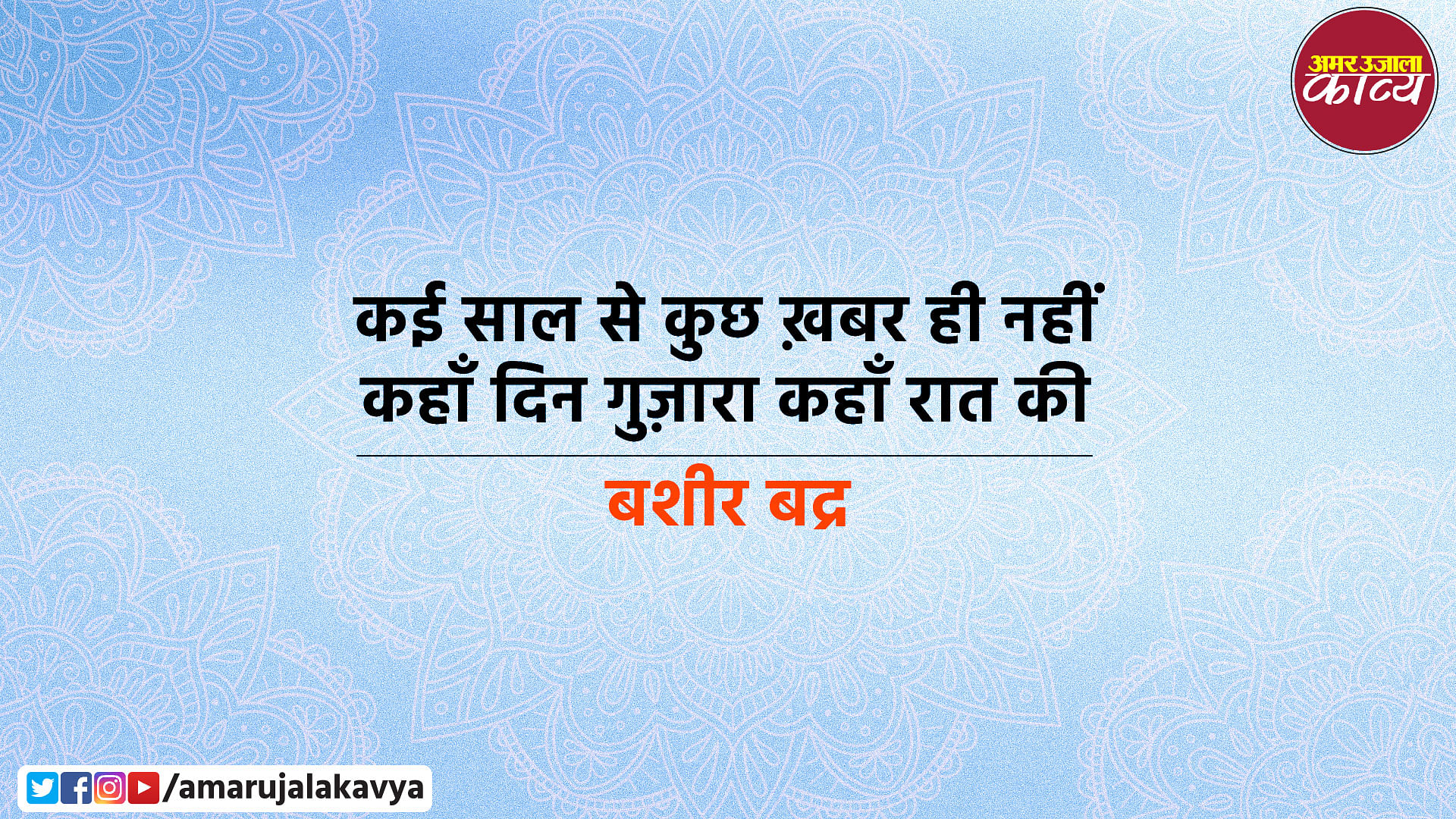
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें